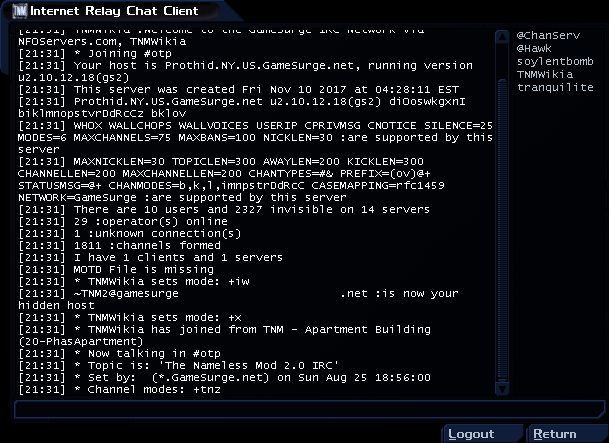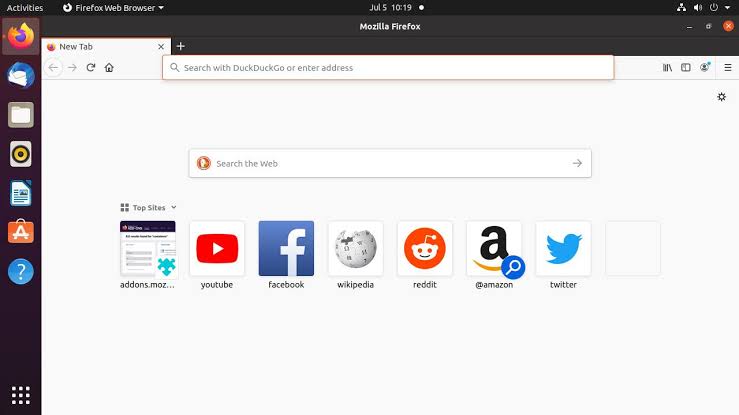माइक्रो कम्प्यूटर या पर्सनल कम्प्यूटर का आधार माइक्रोप्रोसेसर हो है। पुराने दिनों में कम्प्यूटर एक बड़े ट्रक के आकार का होता था तथ्य उनमें प्रयुक्त तार को लम्बाई दिल्ली तथा कालकता के मध्य की दूरी के बराबर हुआ करती थी।
माइक्रोप्रोसेसर के विकास के साथ ही कम्प्यूटरों के आकार डस्क तथा स्थलों के बराबर हो गये तथा अब तो कम्प्यूटर आपको कलाई घड़ी में भी अन्त:स्थापित (embedded) होने लगे।
कम्प्यूटरों को अधिक परियल तथा तेज बनाने में माइक्रोप्रोसेस का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि आज कई प्रोसेसर निर्माता जैस मोटोरोला, ए.एम.डी. इत्यादि है परन्तु इन्टेल को प्रोसेसर निर्माण में पथप्रदर्शक की संज्ञा दी जाती है
आज भी यह सर्वोत्तम स्थान पर आसीन है।इण्टेल 4004 (Intel 4004) इण्टेल 4004 विश्व का पहला माइक्रोप्रोसेसर था जिसे सन 1971 में जारी किया गया था। इसमें 2300 ट्राजिस्टर्स लगे थे और इसका उद्देश्य इस कैल्कुलेटर में प्रयोग करना था।
यह विटा में प्रोसेस करता था, लेकिन इसके निर्देश डाटा 8 बिट सम्बे होते थे। प्रोग्राम और दादा मारी अलग अलग होती थी। इसमें सोलह 4-बिट (या आठ 8 बिट) सामान्य उद्देशीय राजस्टर होते थे। इण्टेल 4004 में 46 निर्देश (nstruction) होते थे।
1) इण्टेल 4040 (Intel 4040) – इण्टेल 4040 इण्टेल 4004 का विस्तारित प्रोसेसर था। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गेम्स, परीक्षण, विकास तथा नियंत्रण उपकरण में होता था। 4040 का पैकेज 4004 से दोगुना चौड़ा था। इसमें 4004 के 16 दिनों के मुकाबले 24 पिन थे।
4040 में 14 इंस्ट्रक्शन जोड़े जाने के अतिरिक्त बड़े (४ लेवल) स्टेक, 8 किलोबाइट प्रोग्राम मेमारी तथा पहले 8 रजिस्टर की shadows सहित इंटरप्ट क्षमताएँ (Interrupt capabilities) था।
2) इण्टेल 8008 (Intel 8008) – इण्टेल 8008 सबसे पहला 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था। इसका कोड नाम 1202 था। इस माइक्रोप्रोसेसर को कन्ट्रोल टर्मिनल कॉरपोरेशन (Control Terminal Corporation) के लिये टर्मिनल कन्ट्रोलर में प्रयोग हेतु बनाया गया था।
8008 इण्टेल के लिये एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदलाव था। इसी के कारण बाद में एक शक्तिशाली 8080 प्रोसेसर का निर्माण संभव हुआ जिसमें 800% इंस्ट्रक्शन सेट थ
3) इण्टेल 8080 (Intel 8080) – इण्टेल 8080 इण्टेल 800% का उतरवत (successor) था। 8080 में एक 16-बिट ऐड्स बस तथा एक 8 बिट डाटा यस थी। इसमें 8 बिट के सात रजिस्टर (छ: को तीन 16-बिट रजिस्टर के रूप में समायोजित किया जा सकता था)
मेमोरी के एक 16-बिट स्टैक प्वाइन्टर (जिसने 8008 के आन्तरिक स्टेक का प्रतिस्थापित किया था) तथा 16-बिट प्रोग्राम काउन्टर थे। इसमें 256 आई ओ पारस (I/O ports) थे। अतः इनपुट आउटपुट डिवाइस को संयोजित करने के लिए किसी ऐसिंग स्पेस (addressing space) के आवंटन को आवश्यकता नहीं थी
जैसा कि मेमारी मैण्ड डिवाइस में आवश्यक था तथा एक पिन थी जिसकी सहायता से स्टैफ अधिकृत मेमारी के अलग बैंक (hank) को अधिकृत कर पाता था। इसके तुरंत बाद ही मोटायला 6800 आया।
4) इण्टेल 8086 (Intel 8086) – इण्टेल 8086 पुरान आई.बी.एम. पर्सनल कम्प्यूटरों में प्रयोग हावाला 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर था। इण्टल 8086 एक ही रजिस्टर के साथ इण्टल 8080 तथा एपटेल 8085 डिजायन पर आधारित था, परन्तु इसे 10 बिट में विस्तारित किया गया था।
5) इण्टेल 8088 (Intel 8088) – इण्टेल 8088 16-बिट रजिस्टर तथा 8 बिट डाटा बस के साथ इण्टेन 8086 का हो विकसित रूप था। 8088 आई.बी.एम पर्सनल कम्प्युटर में प्रयोग होने वाला प्रोसेसर था।
6) इण्टेल 80186 (Intel 80186) – इण्टेल 80186 माइक्रोप्रोसेसर इण्टेल के द्वारा लगभग 1982 में विकसित किया गया था। 80186 इण्टेस 8086 तथा इण्टल 8088 प्रोसस का हुआ रूप था।
इसमें 16-बिट बाहरी बस (External Bus) चे तथा यह 8 बिट या डाटा बस के साथ इण्टेल 80188 के रूप में भी उपलब्ध था। 80186 तथा 80188 के प्रारम्भिक क्लॉक रेट 6 मेगाहर्ज था।
ये बहुत सारे कम्प्यूटरों में प्रयोग नहीं किए जाते थे परन्तु इसमें एक उल्लेखनीय अपवाद (exception) माइण्डस्ट (MMindset) था जो उस समय का अत्याधुनिक कम्प्यूटर था। इसका प्रयोग इम्बेडेड (Embedded) प्रोसेसरों की भांति होता था।
7) इण्टेल 80188 (Intel 80188) – इण्टेल 80188 8 बिट एक्सटर्नल डाटा बस के साथ इण्टेल 80186 का हो वर्जन था। इसमें 16 बिट के बदले एक्सटर्नल डाटा बम का प्रयोग हुआ था। इससे पेरिफेरलूस (peripherals) को जोड़ना सस्ता था।
8) इण्टेल 80286 (Intel 80286) – इण्टेल 80286 को 286 या 1286 भी कहा जाता है। इस प्रोसेसर को भी इण्टल ने विकसित किया था। 80286 प्रोसेसर में 16 चिट डाटा बस थी तथा मेमोरी मैनेजमेन्ट यूनिट को समाहित करता था
जो मल्टीटास्किंग को एक सीमित मात्रा को अनुमति देता था। 80286 में सेग्मेन्टेड (segmented) ममारी मैनेजमेन्ट यूनिट थो जबकि बाद के प्रोसेसर में पन्ड (paged) मेमोरी मैनेजमेन्ट यूनिट (Memory Management Unit) थी
जो खण्डित एम. एम.यू. (MMU) के पीछे जुड़े थे। 80286 प्रोसेसर का प्रयोग आई.बी.एम. पी.सी.ए.टी. (TBM.PCAT) पर्सनल कम्प्यूटरों के साथ होता था।
9) इण्टेल 80386 (Intel 80386) – इण्टेल 80386 इण्टेल 80286 माइक्रोप्रोसेसर का उत्तरवर्ती (successor) प्रोसेसर था। यह पहला इण्टेल प्रोसेसर था जिसमें 32-बिट डाटा यस तथा ऐड्स बस थी।
यह चार गीगाबाइट (2032 बाइट) मेमोरी को रिफर (refer) कर सकता था, फिर भी आई.बी.एम. पी.सी. में सामान्य रूप से 16 मेगाबाइट अधिक थी।
386 में एक से अधिक एप्लिकेशन प्रोग्राम को एक ही समय में (386 विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक्जिक्यूट हो रहे सेफ मोड का प्रयोग कर एक्जिक्यूट होने की अनुमति थी।
10) इण्टेल 80386SX (Intel 80386SX) – इण्टेल 80386SX इण्टेल 80386 का धीमी गति वाला वर्जन था। इसमें 32-बिट डाटा बस के बजाय 16 बिट डाटा बस का प्रयोग होता था। इसमें 24 बिट का ऐड्स बस थी।
यह 286 से अधिक तेज या तथा उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि यह पूर्ण आकार 386 (full-size 386) की भाँति विद्यमान डॉस एप्लिकेशन्स को चलाने में अधिक Flexibility प्रदान करता था।
11) इण्टेल 486 (Intel 486) – इण्टेल 486 को 1486 या APX80486 या इण्टेल DX4 तथा आमतौर पर इसे 486 ही कहा जाता है। यह इण्टेल CISC माइक्रोप्रोसेसर की श्रृंखला में से है
जो इण्टेल 80×86 परिवार के प्रोसेसर का एक अंश था। 486 प्रोसेसर अपने तत्काल पूर्वयत इण्टेल 80386DX के समान था। इसमें मुख्य अंतर यह था कि 486 में एक ओप्टिमाइज्ड (optimised) इन्स्ट्रक्शन सेट था
इसमें ऑन-चिप इंटीग्रेटेड इन्स्ट्रक्शन तथा डाटा कैशे (data cache), एक वैकल्पिक ऑन-चिप फ्लोटिंग प्वाइन्ट यूनिट (Floating Point Unit) तथा एक विस्तारित यस इन्टरफेस इकाई था।
इन सुधार ने समान क्लॉक रेट (clock rate) पर ही इसकी कार्यक्षमता को लगभग दोगुना कर दिया। 486 का उत्तरवर्ती प्रोसेसर पेन्टियम था।
12) पेण्टियम (Pentium) – पेण्टियम 486 का इण्टेल सुपरस्केलर (superscalar) उत्तरवर्ती (successor) था। इसमें 32-बिट 486 टाइप के निर्भरता जाँच (dependency checking) के साथ इंॉटजर पाइपलाइन्स थे।
यह एक चक्र (cycle में अधिकतम दो निर्देशों को एक्जिक्यूट कर सकता थी। बल पाइपलाइन्ड फ्लोटिंग प्वाइन्ट करता था तथा शाखा अनुमा (branch prediction) भी सम्पन्न करता था।
इसमें 16 किलोबाइट ऑन-चिप केश, 64-बिट मेमोरी इंटरफेस, 8 32-बिर समान रजिस्टर तथा 8 80-बिट फ्लोटिंग प्वाइन्ट रजिस्टर थे। इसका क्लॉक रेट (clock rate) 66 मेगाहर्ज, उम विघटन (heat dissipation) 16 W इंटिजर क्षमता 645 SPECin92, फ्लोटिंग प्वाइन्ट क्षमता 56.9 SPECIp92 थी।
इस पण्टियम इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह 80×80 श्रृंखला का पाँचवाँ प्रोसेसर था।
13) पेण्टियम प्रो (Pentium Pro) – पेण्टियम प्रो इन्टर्नल रिस्क (RISC) आर्किटेक्चर पर आधारित था। यह सिस्क रिस्ट ट्रान्सलेटर (CISC-RISC Translator), त्रि-मार्गोय सुपरस्केलर एक्जिक्यूशन तथा आउट ऑफ ऑर्डर एक्जिक्यूशन (out of order execution) के साथ था।
इसमें ब्रान्च अनुमान (prediction) रजिस्टर से नेमिंग (Renaming) के फीचर तथा यह सुपरपाइपलाइन्ड था। पेन्टियम प्रो 32 बिट सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया था
तथा इस पर 16 बिट सॉफ्टवेयर की गति मुख पेन्टियम की अपेक्षाकृत धीमी थी। इसका उत्तरवर्ती प्रोसेसर पेण्टियम था।
14) (पेण्टियम) II (Pentium II) – पेण्टियम II पेण्टियम प्रो (Pentium Pro) का उत्तरवर्ता (sucessor) था। पेण्टियम इण्टेल 800×86 प्रोसेसर परिवार के पहले के सदस्यों के सभी निर्देशों को एक्जिक्यूट कर सकता था।
इसके चार वर्जन विभिन्न यूज मार्केट को ध्यान में रखकर लाये गये थे। सेलेरॉन (Celeron) उनमें सबसे साधारण तथा सबसे महंगा था। स्टैण्डर्ड पेण्टियम सीधे-सीधे घरों तथा व्यापारिक प्रयोगों के लिए था।
पेण्टियम । जिलॉन (Xcon) उच्च क्षमता वाले व्यापारिक सर्व के लिए था। पेण्टियम II का एक मोबाइल वर्जन था जो पोर्टेबल कम्प्यूटरों के प्रयोग के लिए था।
सभी पेण्टियम I प्रोसेसर्स में मल्टीमीडिया विस्तारक (Multimedia Extensions) तथा एकीकृत स्तर एक तथा स्तर दो नियंत्रक (LI and III Cache controllers) थे।
अतिरिक्त फीचर में अलग से 64 बिट सिस्टम तथा कैशे- बस के साथ डायनामिक एक्जिक्यूशन तथा Dual Independent Bus Architecture थे। पेण्टियम || एक सुपरस्केलर सी.पी.यू. था जिसमें लगभग 7.5 मिलियन ट्रॉजिस्टर थे।
15) पेण्टियम III (Pentium III) – पेण्टियम III इण्टेल कारपोरेशन के पेण्टियम || का उत्तरवर्ती था। यह 1999 में परिचित हुआ। इसका clock rate 500 मेगाहर्ट्ज़ था।
पेण्टियम III का आर्किटेक्चर पेण्टियम II के समान था। इसका बाहरी बस 100 या 133 मेगाहर्ट्ज क्लॉक रेट पर चलाया जा सकता था। इसमें 512 किलोबाइट के सैकण्डरी कॅशे बस रह सकते थे यह विभिन्न पैकेजों में जिनमें SECC2 तथा FC-PGA सम्मिलित थे, आ सकता था।
प्रोसेसरों से सम्बन्धित कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य तालिका 2.2 में प्रस्तुत किये गये है। इस तालिका में प्रोसेसर का वर्ष बस की चौड़ाई, क्लॉक रेट तथा ट्राजिस्टर्स की संख्या प्रदर्शित है।